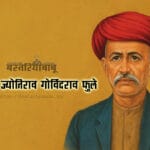भारत का सामाजिक ताना-बाना जाति व्यवस्था के इतिहास से अनछुआ नहीं रहा है। विशेषकर 19वीं सदी के समाज सुधारकों—महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले—ने उस समय की ब्राह्मणवादी पितृसत्ता और जातिगत अत्याचारों के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई थी। उनके जीवन और संघर्षों पर आधारित फिल्म Phule को लेकर हाल ही में जो विवाद उभरा है, वह सिर्फ एक फिल्म के दृश्य संपादन का मामला नहीं है—बल्कि यह सवाल है ऐतिहासिक सच्चाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जातिगत सच्चाइयों के स्वीकार्य या अस्वीकार्य होने का।
फिल्म और विवाद की पृष्ठभूमि –
Phule फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज़ होनी थी, जो महात्मा फुले की जयंती भी है। परंतु सेंसर बोर्ड (CBFC) ने फिल्म में प्रयुक्त कुछ जाति-संबंधी शब्दों—जैसे महार, मांग, पेशवाई, और मनु की जाति व्यवस्था—को “संवेदनशील” करार देते हुए हटाने का आदेश दिया, जिससे फिल्म की रिलीज़ टल कर अब 21 अप्रैल को होने वाली है। यह निर्देश ब्राह्मण फेडरेशन की शिकायत के बाद आया, जिसके अनुसार फिल्म ब्राह्मणों को “नकारात्मक दिखाती है” और “जातिवाद को बढ़ावा देती है।”
क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी के लिए बराबर है?
भारतीय लोकतंत्र की नींव जिस चार मजबूत स्तंभों पर टिकी है—बहस, विचार, असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता—वह हमें संविधान से मिली सबसे मूल्यवान धरोहरों में से एक है। हमें बताया गया कि हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और हर समाज को अपनी संस्कृति, इतिहास और अनुभवों को अभिव्यक्त करने का हक है। लेकिन जब यह आदर्श हमारे समाज की वास्तविकता से टकराता है, तो एक दलित-आदिवासी मनुष्य के भीतर एक सवाल कौंधता है — क्या यह स्वतंत्रता वास्तव में हम सबके लिए समान है? या फिर यह किसी खास वर्ग, खास जाति या खास दृष्टिकोण की जागीर है?
जब कोई ब्राह्मणवादी इतिहास अपनी गौरवगाथा फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और पाठ्यपुस्तकों में खुलकर कहानियाँ रचता है, तो उसे “संस्कृति” और “गौरव” कहा जाता है। लेकिन जब कोई दलित या आदिवासी अपनी पीड़ा, अपनी स्मृति और अपने संघर्षों को दिखाने का प्रयास करता है — तो उसे “आपत्तिजनक”, “संवेदनशील”, या “विवादास्पद” ठहरा दिया जाता है। हमें चुप रहने को कहा जाता है, ताकि दूसरों की भावनाएँ आहत न हों। लेकिन हमारी भावनाओं का क्या? हमारे पूर्वजों पर हुए अत्याचारों, हमारे जीवन की रोज़मर्रा की अपमानजनक सच्चाइयों, और हमारी सांस्कृतिक अस्मिता के लगातार हो रहे दमन का कोई मोल नहीं?
जब हम पूछते हैं कि क्यों हमारे नायकों को इतिहास में जगह नहीं दी गई, तो हमें “एकता” की दुहाई दी जाती है। जब हम अपने पुरखों के संघर्ष की गाथा फिल्मों में दिखाना चाहते हैं, तो सेंसर बोर्ड ‘कट’ का फरमान सुना देता है। आखिर यह किसकी एकता है? यह किसकी भावनाएं हैं? और यह किसका इतिहास है?
हम यह नहीं कहते कि केवल हमारे अनुभव ही सत्य हैं, लेकिन हम यह ज़रूर पूछते हैं — क्या हमारे अनुभव को भी सत्य मानने की जगह है इस लोकतंत्र में?
हमें संविधान ने अधिकार दिया है बोलने का, लिखने का, अपने इतिहास को सहेजने का। लेकिन जब हम इस अधिकार का उपयोग करते हैं, तो पूरा सत्ता तंत्र हमें चुप कराने के लिए खड़ा हो जाता है। कभी सेंसर बोर्ड की आड़ में, कभी ‘धार्मिक भावनाओं’ के नाम पर, और कभी सामाजिक सौहार्द्र के बहाने। असल में यह सत्ता के उस डर का नाम है जो हमारी चेतना से कांपती है — क्योंकि जब दलित-आदिवासी अपने असली इतिहास को जानता है, पहचानता है, और उसे अभिव्यक्त करता है, तो यह व्यवस्था हिलती है।
हम पूछते हैं — क्या लोकतंत्र सिर्फ एक मतपत्र तक सीमित है? क्या संविधान का “We The People” सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? क्या हमारी आवाज़ें, हमारी स्मृतियाँ, हमारे नायक — इस राष्ट्र की परिभाषा में शामिल नहीं?
इसलिए जब कोई कहता है कि फुले जैसे नायक की फिल्म में इस्तेमाल हुए शब्द “संवेदनशील” हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि यह केवल शब्दों को नहीं काटा जा रहा — यह हमारी आत्मा को चीरने की कोशिश है। यह हमें यह बताने का प्रयास है कि तुम केवल शोषित रहो, अपने इतिहास को भूल जाओ, और चुप रहो।
Phule: अभिव्यक्ति या असहजता का कारण?
जब कोई फिल्म सिर्फ मनोरंजन न होकर समाज की अंतरात्मा को झकझोरने का माध्यम बन जाए, तो वह महज़ एक फिल्म नहीं रह जाती — वह एक आंदोलन बन जाती है। Phule ऐसी ही एक फिल्म है। यह जोतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की उस क्रांतिकारी विचारधारा को चित्रित करने का प्रयास करती है, जिसने भारतीय समाज की चीर-फाड़ कर जातिवादी शोषण के ढांचे को सामने लाया। यह फिल्म केवल दो व्यक्तियों की जीवनी नहीं है, यह एक विचारधारा का दस्तावेज़ है — एक ऐसी विचारधारा जो सदियों से कुचले गए, बहिष्कृत और उपेक्षित समुदायों को हक और सम्मान की चेतना देती है। यह फिल्म उन ऐतिहासिक घटनाओं को सामने लाती है जिन्हें मुख्यधारा ने या तो मिटा दिया, या जानबूझकर उपेक्षित किया। यह Phule फिल्म का साहस है कि वह पेशवाई के दमन, मनुवादी जाति व्यवस्था के क्रूर चेहरे, और ‘महार’ व ‘मांग’ समुदायों की पीड़ाओं को बिना संकोच के दृश्य रूप में प्रस्तुत करती है।
जब यह फिल्म समाज के सामने वह आईना रखती है जिसमें भारत को अपने इतिहास के क्रूर सच को देखना होता है — तब कुछ वर्गों में बेचैनी होने लगती है। Phule पर हमला तब शुरू हुआ जब कुछ ब्राह्मण संगठनों ने इसमें प्रयुक्त शब्दों जैसे — ‘महार’, ‘मांग’, ‘पेशवाई’, ‘मनु की जाति व्यवस्था’ — को “आपत्तिजनक” और “संवेदनशील” बताकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से शिकायत की।
इन शिकायतों के आधार पर CBFC ने फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया कि इन शब्दों को फिल्म से हटा दिया जाए।
क्या शब्द आपत्तिजनक हैं या असहज करने वाले?
यह सवाल यहीं से शुरू होता है — क्या ये शब्द वास्तव में आपत्तिजनक हैं, या फिर वे सत्ताधारी मानसिकता को असहज करते हैं क्योंकि वे उस सच्चाई को उजागर करते हैं जिसे सदियों से दबाया गया? ‘महार’ और ‘मांग’ कोई गाली नहीं, बल्कि ऐतिहासिक समुदायों के नाम हैं — वे समुदाय जो सदियों तक अछूत कहे गए, जिनसे पानी छीन लिया गया, शिक्षा और मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। ‘पेशवाई’ एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसने जाति आधारित भेदभाव को संस्थागत रूप दिया। और ‘मनु की जाति व्यवस्था’ केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि इसने एक सामाजिक पिरामिड खड़ा किया जिसमें दलितों को मानवता से बाहर खड़ा किया गया।
तो सवाल यह है — इन शब्दों को हटाने की मांग क्या केवल एक “भावनात्मक” प्रतिक्रिया है, या यह इतिहास को मिटाने की एक साजिश है?
यह केवल सेंसरशिप नहीं, यह स्मृति विलोपन है –
इन शब्दों को फिल्म से हटाने का अर्थ है — स्मृति-विलोपन (Memory Erasure)।
जोतिराव फुले ने अपने समकालीन समाज की सड़ी-गली जातिवादी नींव को चुनौती देने के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने “पेशवाई ब्राह्मणवाद” को उजागर किया, मनु की नीतियों का विरोध किया और ‘महार’ समुदाय के साथ मिलकर शिक्षा और समानता की लड़ाई लड़ी।
इन शब्दों को हटाना न सिर्फ फिल्म के सत्य को नष्ट करता है, बल्कि एक संपूर्ण समुदाय की ऐतिहासिक स्मृति, संघर्ष की चेतना, और आत्मसम्मान के आधार को भी मिटा देने जैसा है।
दलित-आदिवासी समाज के लिए यह सिर्फ फिल्म नहीं — पहचान की लड़ाई है –
जब हाशिए पर खड़े समाज को अपने इतिहास को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिलता है, तो यह महज़ एक फिल्म नहीं रह जाती — यह एक पहचान की लड़ाई बन जाती है। फुले की विरासत सिर्फ शिक्षा की नहीं, बल्कि मनुवादी सोच को खंडित करने की है। वह विरासत आज जब बड़े पर्दे पर आती है, तो सत्ता-संरचना घबराती है। दलित-आदिवासी समाज के लिए Phule का हर दृश्य, हर संवाद, हर ऐतिहासिक संदर्भ — एक स्मरण है, एक उद्घोषणा है कि “हमारा भी इतिहास है, और हम उसे जानना और दिखाना चाहते हैं।”
लेकिन क्या देश तैयार है सच्चाई का सामना करने को?
अगर आज भी हम इन शब्दों से डरते हैं, अगर हम ‘महार’ या ‘पेशवाई’ जैसे ऐतिहासिक संदर्भों को सेंसर कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अब भी उसी डर और संकोच में जी रहे हैं जो जातिवाद ने हमारे भीतर रोप दिया था। क्या हमारी लोकतांत्रिक चेतना इतनी कमजोर है कि वह असहमति, आत्मालोचना और ऐतिहासिक पुनर्पाठ को सहन नहीं कर सकती? फिल्म Phule हमें मजबूर करती है कि हम अपने ऐतिहासिक झूठ को पहचानें, और उस सच्चाई को जगह दें जिसे दशकों से दबाया गया। इसे सेंसर करना केवल एक फिल्म को काटना नहीं है — यह पूरे समाज को अंधकार में ढकेलने जैसा है।
यह सिर्फ फिल्म नहीं, विचारों की लड़ाई है –
Phule फिल्म के इर्द-गिर्द खड़ा हुआ विवाद यह बताता है कि आज भी भारत में जाति व्यवस्था एक ज्वलंत, लेकिन दबा हुआ सच है। यह विवाद कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह उस लंबी लड़ाई का हिस्सा है जो सदियों से शोषित वर्ग अपने अधिकार, अस्मिता और इतिहास की पुनर्प्राप्ति के लिए लड़ रहा है। यह सिर्फ एक फिल्म पर बहस नहीं है — यह विचारों की टकराहट है। एक ओर वे विचार हैं जो जाति के अस्तित्व को नकारना चाहते हैं, उसे मिटा देना चाहते हैं। दूसरी ओर वे विचार हैं जो जाति को पहचानकर, उसकी बुनियाद को तोड़ने का साहस रखते हैं।
हम अक्सर कहते हैं कि “अब तो सब बराबर हैं”, “अब कौन जाति देखता है?” — लेकिन जैसे ही कोई फिल्म, किताब या वक्तव्य जाति आधारित अन्याय की बात करता है, समाज के एक हिस्से में बेचैनी फैल जाती है। यह बेचैनी इस बात की गवाही देती है कि जाति का सच अभी भी जिंदा है — सिर्फ गली-मोहल्लों में नहीं, बल्कि दिमागों में, संस्थाओं में, और यहां तक कि हमारी अभिव्यक्ति की सीमाओं में भी।
लेकिन अब यह चुप्पी टूट रही है।
एक नई पीढ़ी सामने आ रही है — शिक्षित, सचेत, और साहसी –
दलित और आदिवासी समाज आज पहले की तरह नहीं है। अब यह समाज केवल संघर्ष नहीं करता, बल्कि सवाल भी करता है, और जवाब भी चाहता है। यह समाज अब शिक्षा प्राप्त कर रहा है, इतिहास को पढ़ रहा है, अपनी संस्कृति को पुनः खोज रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण — वह अब खुद को अभिव्यक्त कर रहा है।
जो आवाजें पहले मंदिरों से बाहर रोक दी जाती थीं, वे अब किताबों, कैमरों, फिल्मों और विश्वविद्यालयों में गूंज रही हैं।
अब यह समाज पूछता है:
क्यों हमारे नायकों को किताबों में जगह नहीं मिली?
क्यों हमारी संस्कृति को ‘लोककथा’ कहकर उपेक्षित किया गया?
क्यों जब हम अपने दर्द को शब्द देते हैं, तो उसे ‘आपत्तिजनक’ कहा जाता है?
सेंसरशिप विचारों को नहीं रोक सकती –
सेंसरशिप के जरिए फिल्मों से शब्द हटाए जा सकते हैं, लेकिन विचारों को नहीं। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का जीवन आज भी उतना ही सशक्त और प्रासंगिक है जितना 150 साल पहले था — शायद उससे भी ज्यादा। उन्होंने न केवल शिक्षा का दरवाज़ा खोला, बल्कि मनुवादी व्यवस्था को चुनौती दी, ब्राह्मणवाद की नींव हिलाई, और शोषितों को आत्मगौरव का अधिकार दिया।
फुले की यह विचारधारा आज किताबों में नहीं, आंदोलनों में जी रही है, कॉलेजों की बहसों में पल रही है, और अब फिल्मों के जरिए चेतना का हिस्सा बन रही है।
सच बोलना गुनाह नहीं है — चाहे वह कड़वा हो, असहज हो, या किसी को ‘अपमानजनक’ लगे। अगर पेशवाई की सच्चाई, मनु की जाति व्यवस्था, और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को उजागर करना किसी को चुभता है, तो समस्या उस विचार में है, जो सदियों से एक पूरी मानव जाति को नीचे दबाकर खुद को ऊँचा मानता आया है।
सच को ‘संवेदनशील’ कहकर दबाया नहीं जा सकता।
सच को ‘विवादित’ कहकर मिटाया नहीं जा सकता।
और सच को ‘सेंसर’ करके रोका नहीं जा सकता।
क्योंकि अब वो समय बीत गया जब दलित-आदिवासी समाज सिर्फ सहता था। अब वह सवाल करता है, लिखता है, फिल्म बनाता है, और इतिहास दोबारा लिखता है।
दलित-आदिवासी और सिनेमा –
भारतीय सिनेमा एक समय से अधिकतर सवर्ण दृष्टिकोण का विस्तार रहा है। दशकों तक फिल्मों में दलित और आदिवासी चरित्र या तो हास्य पात्र रहे, या फिर सहानुभूति बटोरने वाले “बेचारे” किरदार। उन्हें शायद ही कभी नायक की तरह दिखाया गया — विचारशील, संघर्षशील, और ऐतिहासिक रूप से सजग।
जब भी दलित-आदिवासी समुदायों ने अपने जीवन, पीड़ा और प्रतिरोध की कहानियों को स्वतंत्र स्वर में प्रस्तुत करने की कोशिश की, तो यह मुख्यधारा की असहजता का कारण बन गया। फुले फिल्म पर सेंसरशिप की मांग इसी कड़ी का ताज़ा उदाहरण है। लेकिन यह अकेला मामला नहीं है। यह एक लम्बी परंपरा का हिस्सा है — जहाँ सच्चाई को पर्दे से पहले रोक दिया जाता है, जैसे –
1. Sairat (2016):
मराठी फिल्म Sairat न केवल एक प्रेम कहानी थी, बल्कि जातिवादी सामाजिक ढांचे की निर्ममता पर तीखा प्रहार थी। इसमें दो युवा — एक उच्च जाति की लड़की और एक नीची जाति का लड़का — प्रेम करते हैं। समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता, और अंत में यह प्रेम कहानी हिंसा और हत्या में बदल जाती है।
Sairat की सफलता इस बात का प्रमाण थी कि बहुजन संवेदना को भी लोग समझना और महसूस करना चाहते हैं। लेकिन फिल्म की लोकप्रियता के बावजूद, इसे जातिवादी आलोचना, उपेक्षा और कभी-कभी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा।
Jai Bhim (2021):
तमिल फिल्म Jai Bhim ने एक आदिवासी व्यक्ति के पुलिस हिरासत में मारे जाने और एक वकील के न्याय संघर्ष को दिखाया। यह फिल्म सिर्फ एक कानूनी केस नहीं थी, यह हाशिए के समुदायों की व्यवस्था से लड़ाई का दस्तावेज़ थी।
फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना पाई, लेकिन साथ ही कई वर्गों में तीखी प्रतिक्रिया भी हुई। कुछ संगठनों ने इसे संवेदनशील बताया, जबकि कुछ ने ब्राह्मण विरोधी करार देकर विरोध जताया। यह बताता है कि जैसे ही कोई कथा शोषण के केंद्र तक पहुँचती है, वह कला से राजनीति बन जाती है — और यही बात दलित-आदिवासी सिनेमा को खतरनाक घोषित कर देती है।
3. Masaan, Court, Fandry, Kaala and many more:
Fandry (2013) में एक किशोर दलित लड़के के प्रेम और सामाजिक अपमान को इतनी संवेदनशीलता से चित्रित किया गया कि दर्शक भीतर तक हिल गया। लेकिन इसे “मुख्यधारा” में वह स्थान नहीं मिला जो यह डिज़र्व करती थी।
Court (2014) ने न्याय प्रणाली में जाति और वर्ग के प्रभाव को सामने रखा। यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाज़ी गई, लेकिन भारत में सीमित स्क्रीनिंग मिली।
Kaala (2018) में रजनीकांत ने पहली बार एक बहुजन नायक की भूमिका निभाई। इसमें भूमि अधिकारों, झुग्गियों के अधिकार और जाति-धर्म के संघर्ष को केंद्र में रखा गया। फिल्म के रिलीज़ से पहले ही इसके पोस्टर को जलाया गया, और सवर्ण संगठनों ने इसे ‘विभाजनकारी’ करार दिया।
Masaan (2015) ने बनारस की घाटियों में मौजूद जातीय खांचों और यौन नैतिकता के पाखंड को उजागर किया। इसे आलोचनात्मक सराहना मिली, लेकिन लोकप्रिय मंचों पर सीमित पहुंच।
जब कोई फिल्म दलित-आदिवासी दृष्टिकोण से बात करती है, तो वह केवल एक कहानी नहीं कहती — वह सामाजिक संरचना को चुनौती देती है। यही कारण है कि ऐसी फिल्मों को या तो दबा दिया जाता है, या सीमित रिलीज़ में समेट दिया जाता है। इसलिए जब Phule फिल्म को सेंसर करने की बात आती है, तो यह केवल एक दृश्य को हटाने का मामला नहीं होता। यह उस आत्मा को खामोश करने की कोशिश होती है जो सदियों के अपमान, संघर्ष और प्रतिरोध को बयान करना चाहती है।
आज सिनेमा भी विचार और वर्चस्व की एक युद्धभूमि बन चुका है। यह ज़रूरी है कि हम इन फिल्मों को केवल आर्ट फिल्म या फेस्टिवल सिनेमा के फ्रेम में न देखें। बल्कि यह समझें कि यह एक समुदाय की स्मृति, प्रतिरोध और भविष्य की लड़ाई है।
DISCLAIMER –
यहाँ प्रस्तुत सामग्री का उद्देश्य पाठकों को जानकारी, दृष्टिकोण और वैचारिक विविधता उपलब्ध कराना है, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या विचारधारा को प्रोत्साहित या विरोध करना। लेखों में प्रयुक्त सभी संदर्भ, तिथियाँ, आँकड़े और स्रोत लेखक की शोध प्रक्रिया पर आधारित हैं। हालांकि, हमने यथासंभव सत्यता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, फिर भी किसी त्रुटि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
यदि किसी लेख या विचार से आपको आपत्ति है या कोई सुधार सुझाना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपकी राय का सम्मान करते हैं और तथ्यात्मक सुधार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।